शिक्षण प्रविधियां का इतिहास—आधुनिक शिक्षण शास्त्र का उद्गम 'जान एमास कामेनियस' का उद्गम महान ग्रंथ 'ग्रेट डाइडेक्टिक में विस्तृत रूप से मिलता है। शिक्षक को अध्यापन कार्य करते समय छात्रों की ज्ञानेन्द्रियों को जाग्रत करके ज्ञान व समझदारी विकसित करनी चाहिए।
रुसो ने अपने ग्रंथ 'एमील' में प्रकृति, मानव तथा वस्तुओं को शिक्षक की संज्ञा दी है। अर्थात् बालक प्रकृति से सीखता है। उसने विभिन्न सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। यथा क्रियाशीलता या 'करके सीखने का सिद्धांत, प्रयोग द्वारा सीखना, निरीक्षण द्वारा सीखना आदि बातें प्रस्तुत की।
रूसो के शिष्य पेस्टालाजी ने अनुदेशन (निर्देशन) को मनोवैज्ञानिक बनाने पर बल दिया है। उन्होने प्रतिपादित किया कि शिक्षा अत्तर्निहित शक्तियों को बाहर निकालको की प्रक्रिया है। पेस्टालॉजी के शिष्यों फोबेल तथा हरबर्ट ने उनकी इस विचारधारा को आगे बढ़ाया।
फ्रोबेल ने किंडरगार्डन पद्धति को और हरबर्ट ने अनुदेशन विधि को जन्म दिया हरबर्ट ने अपनी पद्धति के चार पदों को स्थान दिया।(i) स्पष्टता (ii) संबंध (iii) व्यवस्था (iv) विधि हरबर्ट के शिष्य जिलर ने स्पष्टता नामक पद को दो भागों में विभक्त किया प्रस्तावना व प्रस्तुतीकरण यह पांच पद हरबर्ट की पंचपदी के नाम से विख्यात है। मैडम मारिया मोंटेसरी ने स्वशिक्षा को सर्वोच्चता प्रदान की ।फोबेल ने खेल द्वारा शिक्षा को आधार बनाया। जान ड्यूबी ने अनुभव द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया।
पर्यावरणीय अवधारणाओं के स्पष्टीकरण हेतु शिक्षण प्रविधियां
(1) प्रयोग प्रदर्शन विधि (Experimentat Demonstration Method)— इस विधि में अध्यापक विषयवस्तु या किसी अवधारणा के स्पष्ट करने के लिए शिक्षण के साथ-साथ उसे संबंधित सभी आवश्यक प्रयोग स्वयं करके दिखाता है। विद्यार्थी अपने-अपने स्थान पर बैठकर ही विभिन्न प्रकार के उपकरणो, प्रयोगों और क्रियाओं को देखते रहते हैं। इस प्रकार जो विषयवस्तु वे सामान्यत केवल सुनते थे उसे अब आखो से देखते भी हैं और प्रभावशाली ढंग से सीखते हैं।
(2) प्रयोग विधि (Experimental Method)— सीखने की प्रक्रिया में 'करके सीखना' सर्वाधिक प्रभावशाली है। बालक द्वारा प्रयोग स्वयं करके नवीन अवधारणाओं को सीखना ही प्रयोग विधी कहलाती है।प्रयोग विधि के अन्तर्गत कक्षा में प्रयोगशाला में या कक्षा के बाहर परिवेश में किया जा सकता है। आवधाक सामग्री परिवेश से एकत्रित्त करके बालक प्रयोग कर सकता है। प्रयोग करके बालक स्वयं निष्कर्ष निकालकर अवधारणाएं विकसित कर सकता है।
(3) प्रयोगशाला विधि— प्रयोगशाला विधि में विभिन्न प्रकार के प्रमाण बालक स्वयं करते हैं एवं अपने अवलोकनों के आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं। अध्यापक उनकी क्रियाओं का समय-समय पर निरिक्षण कर जरूरी सुझाव देते हैं। इस विधि में बालक पर्यावरणीय अवधारणाओं के समझने के लिए बालक अपने परिवेश से वस्तुएं प्राप्त कर प्रयोग करके सीखते हैं।
इस विधि में छात्र किसी अवधारणा को स्पष्ट करने हेतु स्वयं कार्य करता है जिससे प्राप्त ज्ञान स्थाई होता है।
(4) आगमन विधि—"लेन्डन के शब्दों में" "जब कभी हम बालकों के समक्ष बहुत से तथ्य, उदाहरण या वस्तुए प्रस्तुत करते हैं और फिर उनमें स्वयं निष्कर्ष निकलवाने का प्रयास करते हैं, तब हम शिक्षण की आगमन विधि का प्रयोग करते हैं।"
उपरोक्त परिभाषा के अनुसार इस विधि में विशेष तथ्यों या उदाहरणों की सहायता से सामान्य नियम निकलवाया जाता है। आगमन हमारे मस्तिष्क की एक विशेष क्रिया है, जो विशिष्ट वस्तुओं के निरिक्षण हमको सामान्य सत्य अथवा सिद्धांत की ओर ले आती है।
उदाहरण— इस विधि में विभिन्न वस्तुओं जैसे पत्थर, टिन, लोहा आदि का भार पहले वायु में लेते हैं फिर इन्हीं वस्तुओं का भार जल में लेते हैं। इस तरह लौटने की क्रिया बहुत सारी सूत्रों के साथ करने पर अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि "वस्तुओं का भार वायु की तुलना में जल में कम होता है।"
इस विधि में शिक्षण के तीन सूत्रों का प्रयोग किया जाता है।
(ⅰ) ज्ञात से अज्ञात की ओर (ⅱ) विशिष्ट से सामान्य की ओर (iii) स्थूल से सूक्ष्म की ओर
आगमन विधि के चरण या पद— (i) उदाहरणों का प्रस्तुतीकरण(ⅱ) उदाहरणों से निरीक्षण करना (iii) समस्त उदाहरण से किसी खास नियम को बनाना (iv) फिर उस नियम के सत्यापन हेतु अन्य उदाहरण लेकर सत्यापित करना।
गुण— इस विधि में ज्ञान स्थायी होता है क्योंकि विद्यार्थी स्वयं करके सीखता है। यह आनंददायी विधि है इससे बालक में आत्मविश्वास एवं निर्भरता के गुण विकसित होता है। यह पूर्ण वैज्ञानिक विधि है क्योंकि प्रत्यक्ष तथ्यों पर आधारित है। भविष्य में बालक को खोज एवं अन्वेषण हेतु प्रोत्साहित करती है।
दोष— इस विधि में समय अधिक लगता है। यह प्राथमिक स्तर हेतु उपयुक्त है परन्तु उच्च कक्षाओं हेतु उपयोगी नहीं है। इस विधि में निगमन विधि का सहारा लेना पड़ता है।
निगमन विधी—लेण्डन के अनुसार—"निगमन विधि द्वारा शिक्षण में पहले परिभाषा या नियम सिखाया जाता है फिर उसके अर्थ की सावधानी से व्याख्या की जाती है और अंत में तथ्यों का प्रयोग करने के उसे पूर्ण रूप से स्पष्ट किया जाता है"।
सिद्धांत— (i) सामान्य से विशिष्ट की ओर (ii) सूक्ष्म से स्थूल की ओर (iii) अज्ञात से ज्ञात की ओर
निगमन विधि के चरण पद या सोपान— (i) नियम बताया जाना (ii) प्रयोग या उदाहरण प्रस्तुतीकरण (iii) निष्कर्ष (iv) अभ्यास या परीक्षण द्वारा सत्यता।
गुण— ज्ञान शीघ्रता से प्राप्त होता है। अमूर्त विचारों को छात्र जल्दी आसानी से समझ लेते हैं। इसमें समय कम लगता है।
दोष— यह एक अमनोवैज्ञानिक विधि है। इसमें तर्क एवं विचारशक्ति विकास नहीं होता। इसमें रटने की आदत विकसित होती यह अनुकरण पर बल देती है सूझ-बूझ पर नहीं।
टीप: इस विधि के मुख्य विशेषता नियम का अभ्यास कराया जाना है।
आगमन व निगमन विधि में अन्तर
आगमन विधि— (1) यह मनोवैज्ञानिक विधि है।
(2) यह निम्न कक्षाओं के लिए उपयोगी है।
(3) यह उपर की ओर चलने वाली क्रिया है।
(4) यह अध्यापन की उत्तम विधि है।
(5) यह अनुसंधान पर बल देती है।
(6) यह बालक में आत्मविश्वास तर्क एवं चिन्तन का विकास करती है।
(7) यह विशिष्ट उदाहरणों से सामान्य सिद्धांतों की ओर चलती है।
(8)इस विधि से शिक्षण मन्द गति से होता है।
(9)इसमें बालक गरा सामान्य नियम निकाला जाता है।
(10) इसमें बालक अधिक सक्रिय रहते हैं।
(11) उसमें बालक को खोज एवं निरीक्षण का अवसर मिलता है।
(12) इससे बालकों को सिखाने में बहुत समय लगता है।
(13) इसमें रुचि और जिज्ञासा को जागृत किया जाता है।
निगमन विधि— (1) यह अमनोवैज्ञानिक विधि है।
(2) यह उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी है।
(3) यह नीचे को चलने वाली प्रकिया है।
(4) यह अध्ययन की उत्तम विधि है।
(5) यह अनुशरण पर चल देती है।
(6) यह बालक में आत्मविश्वास तर्क एवं चिंतन का विकास नहीं करती।
(7) यह सामान्य सिद्धांतों से विशिष्ट उदाहरणो की ओर बढ़ती है।
(8) इसमें शिक्षण तीव्र गति से होता है।
(9)इसमें बालक को सामान्य नियम बताया जाता है।
(10) इसमें शिक्षक सक्रिय होता है।
(11) इसमें इस तरह का अवसर नहीं मिलता है।
(12) इसमें बालकों को सिखने में कम समय लगता है।
(13) इसमें रुचि और जिज्ञासा को जागृत नहीं किया जाता है।
(6) विश्लेषण विधि (Malytical Alethord)— यह एक खोज करने वाली विधि है जिसमें बालक एक अन्वेषक के रुप में कार्य करता है। जिस बात को समझना को अथवा जिस समस्या का हल करना हो इसे पहले उपयुक्त छोटे खण्डों में इस तरह विभाजित किया जाता है ताकि वह इतनी छोटी हो जाये कि बालक उसे सरलता से समझ सके। इसके पश्चात शिक्षक उचित प्रश्नों दारा तथा अनुकूल वातावरण उपस्थित करके प्रत्येक खण्ड को समझाने का प्रयत्न करता है। बालक उस पर गहराई से विचार करके समस्या के वास्तविक स्वरूप को समझाने में कुशलताप्राप्त करता है। यह विधि विज्ञान, पर्यावरण व गणित के अध्यापन हेतु सबसे उपयुक्त मानी जाती है।
इस विधि के आधारभूत सिद्धांत— (i) समग्र की अपेक्षा खण्डों को समझना सरल हैं। (ii) अज्ञात से ज्ञात की ओर चलना।
गुण— इस विधि में बालक क्रियाशील रहता है।। बालकों में विचारशक्ति बढ़ती है। इसमें अर्जित ज्ञान स्थायी होता है एवं बालकों में आत्मविश्वास बढ़ता है।
दोष—इसमें समय अधिक लगता है। यह एक अमनोवैज्ञानिक विधि है।
(7) संश्लेषण विधि (Synthetical Method)— किसी वस्तु या समस्या को छोटे-छोटे खण्डों में विभाजन करने मात्र से ही उसका सम्पूर्ण ढांचा प्राप्त नहीं हो जाता। अतः विश्लेषण विधि द्वारा प्राप्त खण्डवार जानकारी क्रमबधदरुप से जोड़कर एक निश्चित रूप देकर अवधारणा को समझाया जाता है।
आधारभूत सिद्धांत— (ⅰ) अंश की अपेक्षा पुर्ण को समझना अधिक अच्छा है।
(ii) अनेकता की अपेक्षा एकता में ही अध्ययन को बल मिलता है।
गुण— इस विधि में समय कम लगने के साथ मनोवैज्ञानिक विधि है। इसमें कमजोर छात्र लाभान्वित होते हैं।
दोष— यह रटने की प्रवृत्ति को जन्म देती है इसमें कल्पना शक्ति का कम विकास होता है।
(8) अन्वेषण विधि (Huristic Method) इस विधि के जन्मदाता प्रोफेसर "आर्मस्ट्रांग" है। विज्ञान एवं पर्यावरण को सफल बनाने के इस पद्धति का प्रयोग किया गया। Hewrisco नामक ग्रीक शब्द से इस विधि का विकास हुआ है जिसका अर्थ है मैं स्वयं खोजता हूँ (I find out myself)। इस विधि का मुख्य उद्देश्य बालकों में अन्वेषण प्रवृति को जागृत करना है। तथा छात्र को चिन्तन, अवलोकन, निरीक्षण व प्रयोग तथा परीक्षण कर सही निष्कर्ष निकलवाना है।
शिक्षाशास्त्री हरबर्ट स्पेन्सर के अनुसार — "बालकों को कम से कम बताना चाहिए और उन्हें अधिक से अधिक स्वयं खोज निकालने के लिए प्रेरित होना चाहिए।"
आर्मस्ट्रांग के अनुसार— "अनुसंधान विधियाँ शिक्षण की वे विधियां हैं जिनमें हम छात्रों को यथासम्भव एक अनुसन्धानकर्ता या खोजों की स्थिति में रखना चाहते है।
अन्वेषण विधि के सिद्धांत—(ⅰ) करके सीखना (ii) मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण (iii) वैज्ञानिक दृष्टिकोण (ⅳ) क्रियाशीलता
गुण— इस विधि से बच्चों में चिंतन करने, सोचने-विचारने की शक्ति का विकास होता है। इससे सीखा ज्ञान स्थाई होता है। इसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास के साथ-साथ आत्मानुशासन आत्मसंयम एवं आत्मविश्वास जागृत होता है।
दोष— यह प्रतिभावान छात्रों हेतु ही उपयुक्त है तथा छोटी कक्षाओं लिए उपयुक्त नहीं है। यह विधि खर्चीली है।
(9) पर्यटन विधि (Excursion Method)— इस विधि के जनक 'पेस्टालाजी' है। यह विधि प्रकृति दर्शन पर आधारित है। पेस्टालॉजी के अनुसार- " पर्यटन बालक को शिक्षा का महत्वपूर्ण साधन है।" पर्यटन एक ऐसा साधन है जिससे द्वारा छात्र अपने ज्ञान को प्रत्यक्षतः देखकर स्थायी व सुदृढ बनाता है।
उदाहरण— जल में रहने वाले जीवों के लिए जलाशय के किनारे ले जाकर बच्चों के प्रत्यक्ष भ्रमण कराया जाता है। इसी तरह तालाब, नदी, पर्वत, श्रृंखला, वाटिकाएँ, मुर्गीपालन केन्द्र, स्वास्थ्यकेन्द्र, रेलवे स्टेशन आदि का भ्रमण कराया जा सकता है।
गुण— पर्यावरण के प्रति अभिरुचि का विकास होता है। बालकों में निरिक्षण शक्ति व वैज्ञानिक सोच का विकास होता है।
दोष— इस विधि में समय अधिक लगता है एवं प्रत्येक प्रकरण इस विधि से नहीं पढ़ाया जा सकता।
(10) समस्या समाधान विधि—वुड के अनुसार "समस्या समाधान वह विधि है जिसके द्वारा सीखने की प्रक्रिया को उन चुनौतीपूर्ण स्थितियों के सृजन द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है, जिसका समाधन करना आवश्यक है।
इस विधि का प्रयोग बालकों में किसी समस्या को हल करने की क्षमता विकसित करने के लिए किया जाता है। इस विधि में बालक समस्या का चयन करते हैं उसके कारणों की खोज करते हैं। उचित मूल्यांकन के पश्चात समस्या का हल ढूंढ़ते हैं।
समस्या समाधान विधि के चरण—
(i) समस्या का चयन
(ii) समस्या चयन का कारण
(iii) समस्या समाधान के लिए कार्ययोजना
(iv) समस्या का हल निकालना
(v) समस्या समाधान का प्रयोग अपने जीवन में करना।
गुण— यह बालकों के भावी जीवन की समस्याओं को हल करने का प्रशिक्षण देती है एवं बालकों में बिचार शक्ति एवं निर्णयशक्ति का विकास करती है। इस विधि में छात्रों में आत्मविश्वास जागृत होता है।
दोष— प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है। इस विधि में यह आवश्यक नहीं कि बच्चे सही समाधान ही निकाल सकें। इस विधि में योग्य शिक्षक को कार्य करा सकते हैं। इसका आवश्यकता से अधिक प्रयोग वातावरण को नीरस बना देता है।
(11) साक्षात्कार विधि—(Interview-Method) साक्षात्कार एक आत्मनिष्ट विधि है जिसके द्वारा छात्रों की समस्याओं तथा गुणो का ज्ञान प्राप्त किया जाता है । इस विधि में शिक्षक और छात्र में आमने-सामने वार्तालप होता है जिसके द्वारा छात्र की समस्याओं का समाधान खोजने तथा शारीरिक और मानसिक दशाओं का ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है।
गुण— (i)इस विधि में अमूर्त घटनाओं का अध्ययन किया जाता है।
(ii) दुसरे के मनोभावों को समझने का कौशल विकसित होता है।
दोष— प्रत्येक प्रकरण को साक्षात्कार विधि से नहीं समझा जा सकता एवं कई अवधारणाएं अन्य विधियों से ही समझी जा सकती हैं।
(12)योजना पद्धति—(Project Method) योजना पद्धति के जन्मदाता अमेरिकी शिक्षाविद 'विलियम हेनरी किलपेट्रिक' है। ये प्रसिद्ध प्रयोगात्मक शिक्षाशास्त्री जान ड्युबी के शिष्य थे।
किल पैट्रिक के अनुसार "प्रोजेक्ट वह सहद्रय सोद्देश्यपूर्ण कार्य है जो पूर्ण संलग्नता से सामाजिक वातावरण में किया जाये"
स्टीवेन्सन के अनुसार "प्रोजेक्ट एक समस्यात्मक कार्य है जिसे स्वाभाविक परिस्थितियों में पूर्ण किया जाता है।"
इस पद्धति में कोई कार्य समस्या के रूप में बालकों के सामने प्रस्तुत किया जाता है और उस समस्या को बालक स्वयं सुलझाने का प्रयास करते हैं।
योजना प्रणाली के आधार भूत सिद्धांत—
(ⅰ) निश्चित प्रयोजन का सिध्दांत
(ii) स्वउत्तरदायित्व का सिद्धांत
(iii) स्वक्रिया का सिद्धांत वास्तविकता का सिद्धांत
(iv) उपयोगिता का सिद्धांत
(v) स्वतंत्रता के सिद्धांत
(vii) सह सम्बंध का सिद्धांत
(viii) सामाजिकता का सिद्धात
योजना पद्धति में सीखने के नियम (i) तत्परता का नियम (ii) प्रभाव का नियम (iii) अभ्यास का नियम
योजना विधि के पद— (i) परिस्थिति का निर्माण (ii) योजना का चुनाव (iii) कार्यक्रम बनाना (iv) योजना को पूर्ण करना (v) योजना का मूल्यांकन (vi) योजना का अभिलेख।
योजना पद्धति के गुण—
(i) स्वतंत्रता।
(ii) जीवनोपयोगिता।
(iii) सामाजिकता का विकास।
(iv) समस्या हल करने की योग्यता का विकास।
(v) सहसम्बंध।
(vi) श्रम की महत्ता को समझना।
(vii) रटने की आदत नही पड़ती।
(viii)व्यावहारिक कुशलता में वृद्धि।
(ix) पर्यावरण के प्रति प्रेम।
(x) विभिन्न गुण जैसे धैर्य, आत्मसंतोष आदि गुणों का विकास
दोष— (i) महंगी है।
(ii) इससे जांच एवं परीक्षा का कोई स्थान नहीं है।
(iii) छोटी कक्षाओं हेतु अनुपयुक्त।
(iv) प्रत्येक प्रकरण पढ़ाना संभव है।

(13) पुस्तकालय विधि (Library Method)— पुस्तकालय विधि में बच्चों को पर्यावरणीय अवधारणा एवं विविध घटनाओं के स्वअध्ययन हेतु इस विधि का प्रयोग किया जाता है। इसमें पुस्तकालय में जाकर बच्चे विभिन्न लेखकों की पुस्तकों का बालक अध्ययन करते है तथा किसी अवधारणा को समझते हैं। पुस्तकालय में विभिन्न पर्यावरणीय पत्र-पत्रिकाएँ भी रखी जाती है जिसका वर्तमान घटना चक्र बच्चों को पता चलता रहता है।
क्रमशः ———


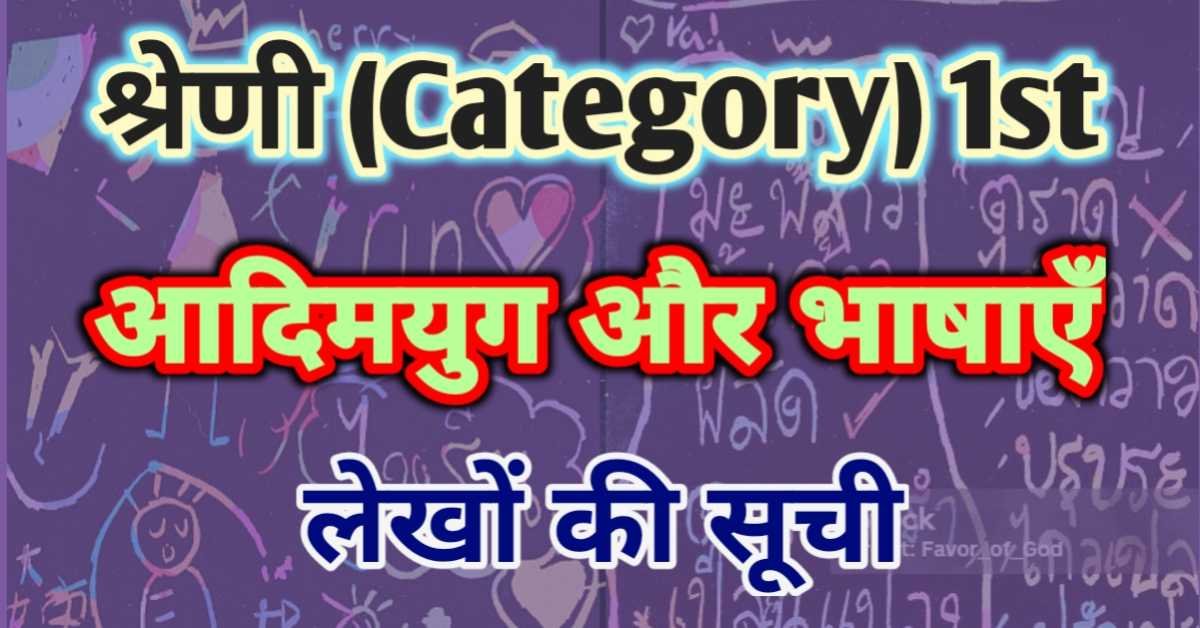
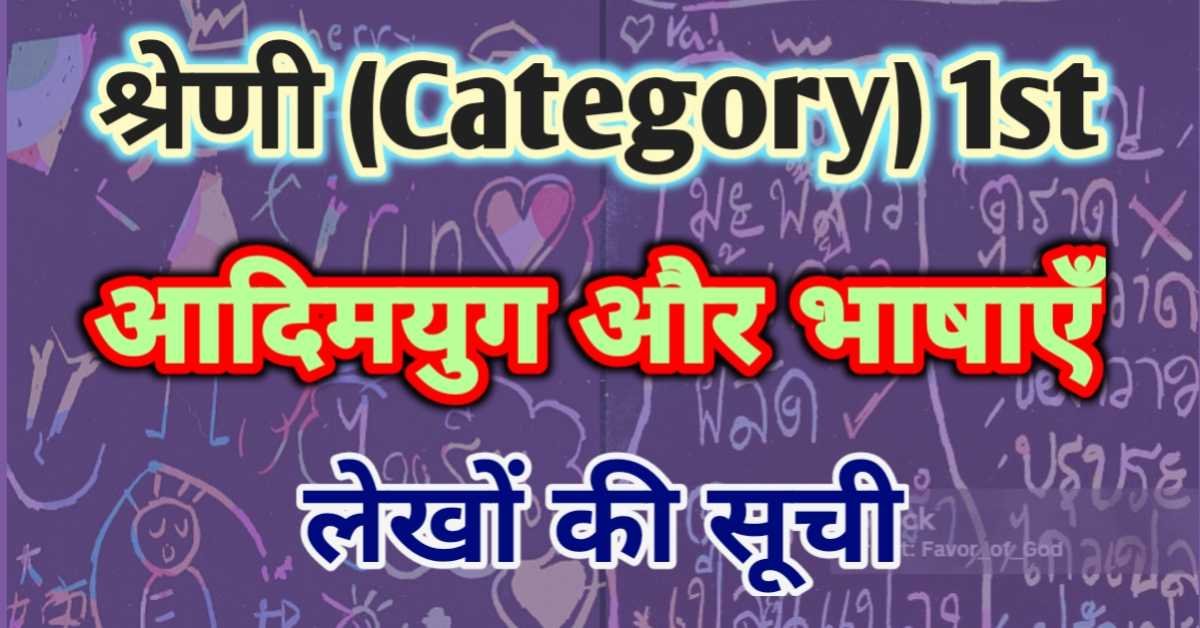
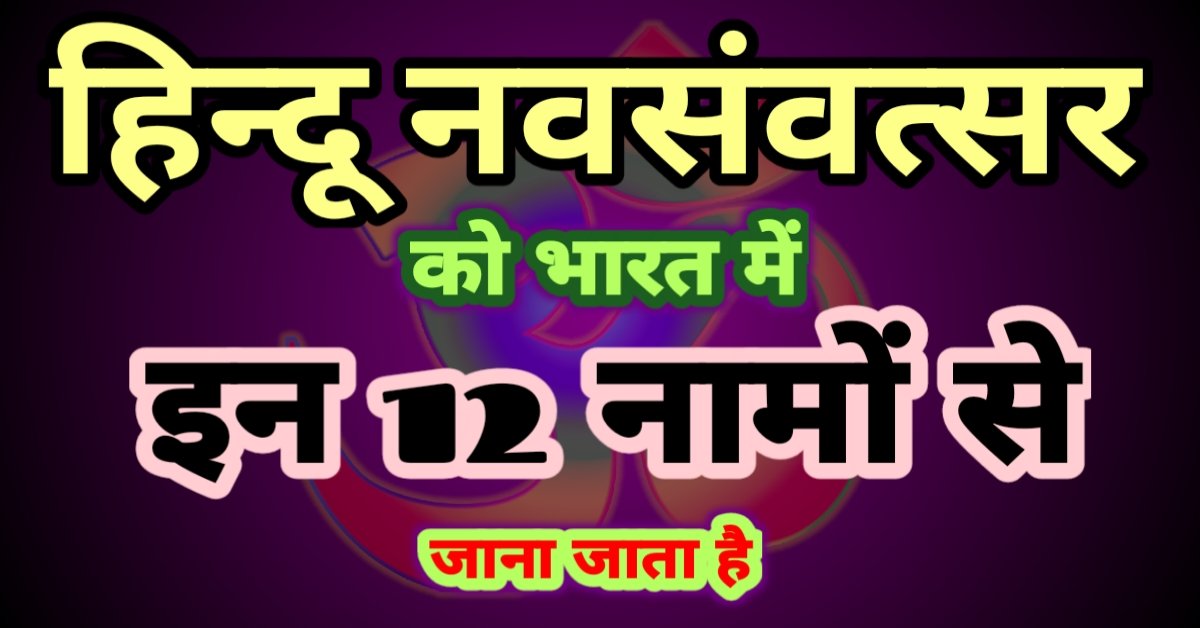
पब्लिक 💬 टिप्पणियाँ (Comments) (0)
अभी तक कोई टिप्पणी नहीं है। पहली टिप्पणी करें!
अपनी टिप्पणी (Comment) दें। 👇