(4) प्रभु प्रलाप सुनि कान बिकल भए बानर निकर
आइ गयउ हनुमान जिमि करुना मुँह बीर रस ॥
संदर्भ― प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य-पुस्तक 'आरोह' में संकलित 'लक्ष्मण-मूर्च्छा और राम का विलाप' प्रसंग से अवतरित है। इसके रचयिता 'तुलसीदास जी' हैं।
प्रसंग - सोरठा छंद की प्रस्तुत पंक्तियों में कविवर तुलसीदास ने भगवान श्रीराम को एक सामान्य मनुष्य की तरह प्रलाप करते देखकर वानरों के भी व्याकुल होने की बात कही है।
व्याख्या- कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रिय भाई लक्ष्मण की दशा देखकर प्रभु श्रीराम अत्यन्त दुःखी हो प्रलाप करने लगते हैं। वह एक सामान्य मनुष्य की भाँति दुःख से व्यथित हो उठते हैं और उनकी आँखों से अश्रुधारा फूट पड़ती है। प्रभु के प्रलाप को कानों से सुनकर आसपास समूहों में चिन्तित अवस्था में खड़े राम की सेना के वानर भी अत्यधिक व्याकुल हो गये। इतने में ही पवन-वेग से उड़ते हुए हनुमान जी वहाँ पहुँच जाते हैं। उनके आगमन पर ऐसा लगता है मानो अचानक से करुण रस के प्रसंग में वीर रस प्रकट हो गया है। सूर्योदय से पूर्व हनुमान जी को संजीवनी बूटी के साथ देखकर कुछ ही क्षणों पूर्व उदास और दुःखी वानर सेना में नव-उत्साह का संचार हो जाता है।
विशेष (काव्य सौंदर्य) ― (1) हनुमान जी के आगमन से वानर सेना में उत्साह का संचार होता है। (2) सोरठा छंद है। (3) अनुप्रास अलंकार की छटा दर्शनीय है। (4) करुण रस विद्यमान है। (5) तत्सम शब्दावली युक्त अवधी भाषा है।
(5) हरषि राम भेटेउ हनुमाना। अति कृतग्य प्रभु परम सुजाना ॥
तुरत बैद तब कीन्हि उपाई। उठि बैठे लछिमन हरषाई ॥
हृदय लाइ प्रभु भेंटेउ भ्राता। हरषे सकल भालु कपि ब्राता ॥
कपि पुनि बैद तहाँ पहुँचावा। जेहि बिधि तबहिं ताहि लड़ आवा ॥
संदर्भ― प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य-पुस्तक 'आरोह' में संकलित 'लक्ष्मण-मूर्च्छा और राम का विलाप' प्रसंग से अवतरित है। इसके रचयिता 'तुलसीदास जी' हैं।
प्रसंग - करने, लक्ष्मण की मूर्च्छा टूटने और लक्ष्मण के उठ खड़े होने पर राम एवं उनकी पूरी सेना के प्रसन्न होने का सजीव वर्णन किया है।
व्याख्या- कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि हनुमान जी के सूर्योदय से पूर्व ही वहाँ पहुँच जाने पर चारों ओर उत्साह का संचार हो गया। संजीवनी बूटी लेकर आये हनुमान जी को देखकर भगवान राम अपने स्थान से उठ खड़े हुए और हर्षित होकर उन्हें गले लगा लिया। हनुमान जी से मिलकर अत्यन्त ज्ञानवान भगवान श्रीराम ने उनके प्रति अपना कृतज्ञता भाव प्रकट किया। तब तुरन्त ही संजीवनी बूटी को परिष्कृत करके वैद्य सुषेन ने मूर्च्छित लक्ष्मण का उपचार किया जिसका शीघ्र प्रभाव हुआ और लक्ष्मण हर्षित होकर उठ बैठे। लक्ष्मण की मूर्च्छा टूटने और उन्हें प्रसन्नतापूर्वक स्वस्थ पाकर प्रभु राम अपने भाई को हृदय से लगाकर मिले। मेल-मिलाप का यह दृश्य देखकर वहाँ उपस्थित सभी भालू और वानरों के समूह भी प्रसन्नता से झूम उठे। चारों ओर खुशी छा गई। हनुमान जी ने सुषेन वैद्य को उसी प्रकार तथा उसी विधि से वहाँ पहुँचा दिया जिस प्रकार वे उन्हें पहले लेकर आये थे।
विशेष (काव्य सौंदर्य) ― (1) हनुमान जी के सूर्योदय से पूर्व संजीवनी बूटी लेकर पहुँचने पर प्रभु राम कृतज्ञ भाव से उन्हें गले लगा लेते हैं। (2) चौपाई छंद है। (3) अनुप्रास अलंकार की छटा है। (4) तत्सम शब्दावली युक्त अवधी भाषा है।
(6) कथा कही सब तेहिं अभिमानी। जेहि प्रकार सीता हरि आनी ॥
तात कपिन्ह सब निसिचर मारे। महा महा जोधा संघारे ॥
दुर्मुख सुररिपु मनुज अहारी। भट अतिकाय अकंपन भारी ॥
अपर महोदर आदिक बीरा। परे समर महि सब रनधीरा ॥
संदर्भ― प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य-पुस्तक 'आरोह' में संकलित 'लक्ष्मण-मूर्च्छा और राम का विलाप' प्रसंग से अवतरित है। इसके रचयिता 'तुलसीदास जी' हैं।
प्रसंग - प्रस्तुत पंक्तियों में तुलसीदास जी ने रावण-कुम्भकर्ण वार्तालाप का वर्णन करते हुए लिखा है कि रावण अपने भाई कुम्भकर्ण को बताता है कि हनुमान आदि वानरों ने युद्ध में अनेक बड़े राक्षसों को मार डाला है।
व्याख्या- तुलसीदास जी कहते हैं कि कुम्भकर्ण द्वारा रावण से उसके चेहरे पर उभरी चिन्ता की लकीरों का कारण पूछने पर रावण अपने भाई को सारा वृतान्त सुनाता है। उस अभिमानी-घमण्डी रावण ने कुम्भकर्ण को अब तक की पूरी कथा बताई कि किस प्रकार वह सीता जी का अपहरण कर लाया था। रावण अपने भाई कुम्भकर्ण को सम्बोधित करते हुए कहता है कि हे मेरे भाई ! हनुमान आदि वानरों ने सभी राक्षस मार डाले हैं। उन्होंने लंका के बड़े-बड़े महान योद्धाओं का भी संहार कर डाला है। युद्ध में हुई क्षति का वर्णन करते हुए रावण आगे कहता है कि दुर्मुख, देवान्तक, नरान्तक, भारी योद्धा अतिकाय और अकम्पन तथा महोदर सरीखे वीर योद्धा युद्धभूमि में पृथ्वी पर मरे पड़े हैं।
विशेष (काव्य सौंदर्य) ― (1) हनुमान आदि वानरों द्वारा लंका के बड़े-बड़े महान योद्धाओं का चध करने की बात कही गई है। (2) चौपाई छंद है। (3) 'महा महा 'में पुनरुक्तिप्रकाश अलंकार है। (4) 'कथा कही' एवं 'अतिकाय अकंपन' में अनुप्रास की छटा है। (5) वीर रस विद्यमान है। (6) तत्सम शब्दावली युक्त अवधी भाषा है।
पाठ का अभ्यास
कविता के साथ
1. कवितावली में उद्धृत छंदों के आधार पर स्पष्ट करें कि तुलसीदास को अपने युग की आर्थिक विषमता की अच्छी समझ है।
उत्तर - तुलसीदास कृत 'कवितावली' में उधृत छंदों से स्पष्ट पता चलता है कि तुलसीदास जी को अपने युग की आर्थिक विषमता की गहरी समझ थी। समाज के विभिन्न वर्गों में यह आर्थिक विषमता तत्कालीन समाज में व्याप्त अत्यधिक बेकारी के कारण उत्पन्न हुई थी। तुलसीदास जी के अनुसार उनके समय के समाज में हाथों को काम नहीं था। लोग काम-धन्धे के अभाव में अत्यन्त दुःखी थे। किसान के लिए खेती की व्यवस्था नहीं थी। भिखारी के लिए कोई भिक्षा देने वाला नहीं था। व्यापारी के पास व्यापार नहीं था। नौकरों के लिए नौकरी नहीं थी। काम-धन्धा न होने के कारण समकालीन समाज में घर-घर दरिद्रता रूपी रावण अपने पैर जमाए बैठा था। इसी आर्थिक विषमता के कारण ही समाज में ऊँच-नीच का भाव मौजूद था। दुखी लोग उनके कौशल का काम उपलब्ध न हो पाने के कारण निकृष्टतम कार्य करने के लिए भी तैयार हो जाते थे। तुलसीदास जी ने स्वयं आर्थिक विषमता को भोगा और लोगों की दीनावस्था को अपनी आँखों से देखा था। अपने उन्हीं अनुभवों का वर्णन उन्होंने 'कवितावली' में किया है।
2. पेट की आग का शमन ईश्वर (राम) भक्ति का मेघ ही कर सकता है-तुलसी का यह काव्य-सत्य क्या इस समय का भी युग-सत्य है ? तर्कसंगत उत्तर दीजिए।
उत्तर - 'पेट की आग का शमन ईश्वर भक्ति का मेघ ही कर सकता है'- तुलसीदास जी का यह काव्य-सत्य आज के समय में भी सत्य जान पड़ता है। वास्तव में, मनुष्य को अपने पेट की भूख को शान्त करने के लिए पुरुषार्थ करने की आवश्यकता होती है। यदि यह पुरुषार्थ सात्विक भाव के साथ धर्मसम्मत तरीके से किया जाये तो उसके फलीभूत होने की सम्भावना बढ़ जाती है। ऐसे में ईश्वर-स्मरण के साथ किये गये कार्य के परिणाम अधिक सन्तोषजनक और स्थायी होते हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि आज के इस घोर कलयुग में भी पेट की आग की पूर्ति के लिए उद्यम के साथ-साथ धर्म रूपी ईश्वरीय भक्ति का वरदान भी अति आवश्यक है।
3. तुलसी ने यह कहने की जरूरत क्यों समझी ?
धूत कहौ, अवधूत कहौ, रजपूतु कहौ, जोलेहा कहौ कोऊ काहू की बेटीसों बेटा न ब्याहब, काहूकी जाति बिगार न सोऊ। इस सवैया में काहू के बेटासों बेटी न ब्याहब कहते तो सामाजिक अर्थ में क्या परिवर्तन आता ?
उत्तर - कवि तुलसीदास जी को उपर्युक्त कथन कहने की आवश्यकता इसीलिए पड़ी क्योंकि उनके समय में जातिवाद का अत्यधिक बोलबाला था। कई जातियों को अन्य की तुलना में हीन अथवा गौण माना जाता था तथा ऐसी जातियों के साथ सामाजिक रूप से भेदभाव किया जाता था। लोगों ने तुलसीदास जी की जाति-धर्म पर प्रश्न उठाते हुए आक्षेप लगाये थे जबकि तुलसीदास राम की भक्ति में लीन एक संन्यासी अथवा सन्त थे। और जैसा कि सभी जानते हैं कि साधु की अपनी कोई जाति नहीं होती है इसलिए तुलसीदास जी लिखते हैं कि लोग उन्हें किस जाति अथवा धर्म के मानते हैं इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वह तो जातिवाद के इन झूठे आडम्बरों से परे राम-प्रेम की सीमा में आबद्ध हैं। वे कहते हैं कि उन्हें किसी की बेटी से अपने बेटे का विवाह नहीं कराना है जो किसी की जाति बिगड़ जायेगी।
इस सवैया में यदि तुलसीदास 'काहू के बेटासों बेटी न व्याहब' कहते तो सामाजिक परिदृश्य एवं निहितार्थ बदल जाता है। हिन्दू समाज में बेटी विवाह के उपरान्त पति की जाति (गोत्र) को अंगीकार कर अपने नाम में जोड़ लेती है। ऐसी परम्परा सदियों से चली आ रही है। ऐसे में यदि तुलसीदास अपनी बेटी का विवाह किसी के बेटे से करवाते तो उनकी पुत्री को भी अपने पति की जाति स्वीकार करनी पड़ती। ऐसे में किसी दूसरे के घर में उनकी पुत्री के रूप में उनकी जाति (गोत्र) का प्रवेश हो जाता जो कथित रूप से दूसरे की जाति बिगाड़ना समझा जाता।
4. धूत कहौ.... वाले छंद में ऊपर से सरल व निरीह दिखलाई पड़ने वाले तुलसी की भीतरी असलियत एक स्वाभिमानी भक्त हृदय की है। इससे आप कहाँ तक सहमत हैं ?
उत्तर - रामभक्त तुलसीदास ने विनय सम्बन्धी अनेक कविताओं (छंदों) की रचना की है जिससे वे अत्यन्त सरल, सहज एवं निरीह दिखलाई पड़ते हैं। किन्तु यह सत्य नहीं है। वह स्वाभिमानी कवि हैं। बचपन से ही उन्हें अनेकानेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अत्यल्प आयु में ही माता-पिता का देहान्त हो गया। अनाथ तुलसीदास का विवाह भी छोटी आयु में ही 'रत्नावली' के साथ हुआ। पत्नी प्रेम में डूबे तुलसीदास को पत्नी से भी दुत्कार मिली। इससे उनके अन्दर का स्वाभिमान जाग गया और उन्होंने संन्यास ले लिया। लोगों ने उनकी जाति पर भी आक्षेप लगाये। तब भी स्वाभिमानी तुलसीदास अपने हृदय में राम की भक्ति धारण किये अविचलित रहे और जीवन भर जाति-पाँति और झूठे धार्मिक आडम्बरों का डटकर विरोध करते रहे। अतः यह कहा जा सकता है कि ऊपर से सरल व निरीह दिखलाई पड़ने वाले तुलसीदास वास्तव में अन्दर से एक स्वाभिमानी भक्त हृदय के स्वामी रहे हैं। हम इस तथ्य से पूर्णतः सहमत हैं।
5. भ्रातृशोक में हुई राम की दशा को कवि ने प्रभु की नर लीला की अपेक्षा सच्ची मानवीय अनुभूति के रूप में रचा है। क्या आप इससे सहमत हैं ? तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए।
उत्तर - भ्रातृशोक में हुई राम की दशा को कवि तुलसीदास ने प्रभु की नर लीला की अपेक्षा सच्ची मानवीय अनुभूति के रूप में रचा है। हम इस तथ्य से पूर्णतः सहमत हैं। मेघनाद-लक्ष्मण युद्ध में मेघनाद द्वारा छोड़ी गई शक्ति से लक्ष्मण मूच्छित हो जाते हैं। ऐसे में प्रभु राम का भ्रातृ प्रेम अपने चरम पर पहुँच जाता है। हनुमान जी को संजीवनी बूटी लाने में हो रही देरी और लक्ष्मण की पल-पल बिगड़ती हालत से करुणानिधान द्रवित होकर जनसामान्य की तरह विलाप कर उठते हैं। उन्हें लक्ष्मण की पूर्व की बातें, उनका स्वभाव एवं स्वयं के प्रति लक्ष्मण का त्याग इत्यादि स्मरण हो उठते हैं। अपने सहोदर को अपने सामने काल के गाल में जाता देख श्रीराम एक मनुष्य की भाँति ही चीत्कार कर उठते हैं। धीरे-धीरे उनका विलाप, प्रलाप में बदल जाता है। वे यहाँ तक कह उठते हैं कि यदि उन्हें पता होता कि मुझे अपनी पत्नी के लिए भाई से इस प्रकार बिछड़ना पड़ेगा तो मैं पिताजी की वनगमन की आज्ञा नहीं मानता। वे अपनी पत्नी सीता की हानि को भी विशेष नुकसान नहीं मानते हैं। ऐसे विचार अथवा भाव मर्यादा पुरुषोत्तम राम के कदापि नहीं हो सकते हैं। ये कथन एवं विचार तो एक सामान्य-जन की सच्ची मानवीय अनुभूति के ही परिणाम हो सकते हैं। प्रभु के इतर एक आम आदमी ही 'जग में कलंक लेकर जीना पड़ेगा' एवं 'क्या मुँह दिखाऊँगा' जैसी सांसारिक बातें सोच सकता है।
6. शोकग्रस्त माहौल में हनुमान के अवतरण को करुण रस के बीच वीर रस का आविर्भाव क्यों कहा गया है ?
उत्तर - लक्ष्मण-मेघनाद के युद्ध में मेघनाद द्वारा छोड़ी गई शक्ति से लक्ष्मण मूच्छित हो जाते हैं। राम, लक्ष्मण के मूच्छित शरीर को गोद में रखकर अत्यन्त दुखी हो उठते हैं। हनुमान जी के संजीवनी बूटी लेकर आने में हो रही देरी से उनकी यह व्याकुलता और बढ़ जाती है। आधी रात बीत जाने पर भी जब पवनपुत्र वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं तो राम का यह विलाप, प्रलाप में परिवर्तित हो जाता है। राम को इस प्रकार दुःखी और प्रलाप करता देख समूची राम सेना भी शोकग्रस्त हो जाती है। दृश्य अत्यन्त कारुणिक हो जाता है। अचानक से हाथ में संजीवनी बूटी के स्थान पर पूरा-का-पूरा पर्वत धारण किए हनुमान जी सूर्योदय से पूर्व वहाँ पहुँचते हैं। हनुमान जी के ससमय अवतरण से राम एवं उनकी सेना अत्यन्त प्रसन्न होती है। वैद्य सुषेन लाई गई संजीवनी जड़ी-बूटी से लक्ष्मण का उपचार करते हैं। शीघ्र ही, लक्ष्मण की मूच्छ टूटती है और वह स्वस्थ होकर उठ खड़े होते हैं। यह सब देखकर चारों ओर खुशी और उत्साह का संचार हो जाता है। कुछ समय पूर्व तक वहाँ पसरा करुण रस यकायक से वीर रस में परिवर्तित हो जाता है।
7. जैहउँ अवध कवन मुहुँ लाई। नारि हेतु प्रिय भाइ गँवाई ॥
बरु अपजस सहतेउँ जग माहीं। नारि हानि बिसेष छति नाहीं।।
भाई के शोक में डूबे राम के इस प्रलाप-वचन में स्त्री के प्रति कैसा सामाजिक दृष्टिकोण सम्भावित है ?
उत्तर - भाई के शोक में गहरे डूबे राम के इस प्रलाप वचन में स्त्री के प्रति कहे गये शब्दों को यदि उनके सामान्य अर्थ में ही देखेंगे-समझेंगे तो प्रथम दृष्ट्या यह लगेगा कि उस काल में स्त्रियों के प्रति समाज का दृष्टिकोण उपेक्षा का रहा होगा। किन्तु जैसे ही हम उपर्युक्त प्रलाप वचन की पृष्ठभूमि और परिस्थितियों को समझने का प्रयास करेंगे तो यह पायेंगे कि स्त्रियों के लिए कहे गये ये वचन पहले तो भगवान श्रीराम ने प्रभु की भूमिका में नहीं अपितु एक सामान्य-जन के अंतस की गहरी पीड़ा को अभिव्यक्त करने के समय कहे थे। दूसरे, ये वचन भ्रातृ-शोक से उत्पन्न अत्यन्त शोकग्रस्त अवस्था में राम द्वारा तब कहे गये थे जब वे अत्यन्त व्याकुल एवं अधीर हो प्रलाप कर रहे थे। साथ ही, भाई के प्रति अपने अगाध प्रेम को प्रदर्शित करने हेतु उसके लिए अपनी प्रिय पत्नी सीता तक की हानि सहने के लिए तत्पर राम द्वारा ये वचन कहने का आशय मात्र इतना था कि वे अपने भाई को अपनी पत्नी से भी अधिक प्रेम करते थे। इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि सीता के प्रति उनका प्रेम कम था या फिर स्त्रियों के प्रति उनका श्रद्धाभाव कमतर था। गुस्से, प्रलाप एवं लगभग विवेकशून्य की सी स्थिति में राम द्वारा की गई इस त्वरित टिप्पणी को वास्तव में शब्दों के अर्थ के स्थान पर उनमें छिपे भाव के रूप में देखा जाना चाहिए।
कविता के आस - पास
1. कालिदास के रघुवंश महाकाव्य में पत्नी (इंदुमती) के मृत्यु-शोक पर अज तथा निराला की 'सरोज-स्मृति' में पुत्री (सरोज) के मृत्यु-शोक पर पिता के करुण उद्गार निकले हैं। उनसे भ्रातृशोक में डूबे राम के इस विलाप की तुलना करें।
उत्तर - कालिदास के महाकाव्य 'रघुवंश' में 'अज' के उद्गार अपनी पत्नी की मृत्यु होने पर उत्पन्न शोक में निकले हैं जो पत्नी के प्रति उनके उच्च प्रेम को प्रदर्शित करते हैं। वे पत्नी वियोग में अत्यधिक पीड़ा का अनुभव करते हैं। जबकि महाकवि निराला ने 'सरोज-स्मृति' में अपनी पुत्री 'सरोज' की अनायास मृत्यु पर जो उद्गार व्यक्त किये हैं, वे एक असहाय पिता के उदगार हैं जो उनकी पुत्री के अचानक देहावसान के कारण उपजे थे। उपरोक्त दोनों की तुलना में राम का शोक अपेक्षाकृत कम है। क्योंकि लक्ष्मण अभी तक केवल मूच्छित हैं और उनके उपचार के लिए प्रयास किये जा रहे हैं। हनुमान जी के रूप में राम के पास एक आशा की चमकती किरण है। यदि सूर्योदय से पूर्व हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने में सफल रहे तो लक्ष्मण के प्राण बचाये जा सकते हैं। यद्यपि भ्रातृ-प्रेम में अधीर राम का व्याकुलता भरा विलाप-प्रलाप भीतर तक व्यथित कर देता है।
2. 'पेट ही को पचत, बेचत बेटा-बेटकी' तुलसी के युग का ही नहीं आज के युग का भी सत्य है। भुखमरी में किसानों की आत्महत्या और सन्तानों (खासकर बेटियों) को भी बेच डालने की हृदय विदारक घटनाएँ हमारे देश में घटती रही हैं। वर्तमान परिस्थितियों और तुलसी के युग की तुलना करें।
उत्तर - तुलसीदास जी के समय में लोगों की आर्थिक स्थिति अत्यन्त खराब थी। आज भी सैकड़ों वर्ष बाद भी स्थिति वैसी-की-वैसी ही है। सब ओर बेकारी, गरीबी और लाचारी का बोलबाला है। देश के कई हिस्सों में भुखमरी की स्थिति है। अक्सर ऐसे समाचार देखने, पढ़ने, सुनने को मिलते हैं कि अन्नदाता किसान गरीबी भुखमरी से तंग आकर अपने जीवन की इहलीला को समाप्त कर देते हैं। आज भी देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में रोटियों के लिए बेटियों को बेचा जाता है। ऐसी हृदय विदारक घटनाओं पर तुरन्त रोक लगनी चाहिए। सरकार द्वारा अपने देशवासियों को भुखमरी से बचाने हेतु कड़ा कानून बनाकर भुखमरी से होने वाली हर एक मृत्यु के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करनी चाहिए।
3. तुलसी के युग की बेकारी के क्या कारण हो सकते हैं ? आज की बेकारी की समस्या के साथ उसे मिलाकर कक्षा में परिचर्चा करें।
उत्तर - तुलसीदास जी के युग में बेकारी के कई कारण; जैसे-खेती हेतु सिंचाई की व्यवस्था का न होना, अशिक्षा, अत्यधिक जनसंख्या का दबाव, लोगों में शारीरिक श्रम के प्रति अरुचि, लोगों का कौशल विहीन होना, बार-बार ओलावृष्टि, अकाल, बाढ़ जैसे प्राकृतिक प्रकोप का आना इत्यादि थे। वर्तमान युग में भी बेकारी की समस्या ज्यों-की-त्यों बनी हुई है। सच पूछिए तो पहले की तुलना में कई सौ गुना बढ़ गई है। आज की बेकारी की समस्या के कारण तुलसीदास जी के युग की बेकारी की समस्या के कारणों जैसे ही हैं। कुछेक जो नये कारण पैदा हो गये हैं, उनमें सुनियोजित विकास की नीति का अभाव, पूँजीपतियों द्वारा शोषण, भ्रष्टाचार, सरकारों का उदासीन रवैया, जनसंख्या विस्फोट इत्यादि शामिल हैं।
4. राम कौशल्या के पुत्र थे और लक्ष्मण सुमित्रा के। इस प्रकार वे परस्पर सहोदर (एक ही माँ के बच्चे के पेट से जन्मे) नहीं थे। फिर, राम ने उन्हें लक्ष्य कर ऐसा क्यों कहा - "मिलइ न जगत सहोदर भ्राता" ? इस पर विचार करें।
उत्तर - राम कौशल्या के पुत्र थे और लक्ष्मण सुमित्रा के। भले ही राम और लक्ष्मण एक माँ की कोख से पैदा हुई सन्तानें नहीं थे किन्तु वे सबसे अधिक समय एक-दूसरे के साथ व्यतीत करते थे। लक्ष्मण सदैव परछाई की तरह राम के साथ-साथ रहते थे। राम भी उन्हें अत्यधिक स्नेह करते थे। अपने बड़े भाई के लिए लक्ष्मण ने अपना राज-पाट, माता-पिता, पत्नी सब-कुछ छोड़कर भ्राता राम के साथ वन जाने का निर्णय लिया। जो एक अभूतपूर्व घटना थी। भाई के लिए लक्ष्मण जैसे त्याग का अनुपम उदाहरण मानव सभ्यता के इतिहास में दूसरा नहीं मिलता। दोनों में एक-दूसरे के प्राण बसते थे। इसीलिए आज भी दो भाइयों में अत्यधिक प्रेम देखकर लोग अक्सर कह देते हैं कि तुम्हारी जोड़ी तो 'राम-लक्ष्मण' जैसी है। उपर्युक्त कारणों से ही प्रभु राम ने यह कहा कि लक्ष्मण जैसा सहोदर भाई संसार में कहीं नहीं मिल सकता है।
5. यहाँ कवि तुलसी के दोहा, चौपाई, सोरठा, कवित्त, सवैया-ये पाँच छंद प्रयुक्त हैं। हैं। इसी प्रकार तुलसी साहित्य में और छंद तथा काव्य-रूप आए हैं। ऐसे छंदों व काव्य-रूपों की सूची बनाएँ।
उत्तर - तुलसी साहित्य में दोहा, चौपाई, सोरठा, कवित्त और सवैया छंदों के अतिरिक्त भी कई और छंद देखने को मिलते हैं। इनमें से प्रमुख हैं-बरवै, छप्पय, हरिगीतिका इत्यादि। साथ ही तुलसी साहित्य में विभिन्न अन्य काव्य-रूप भी मिलते हैं। इनमें से कुछ प्रमुख काव्य-रूप निम्नलिखित हैं-
मुक्तक काव्य - विनय पत्रिका।
प्रबन्ध काव्य - रामचरितमानस (महाकाव्य)
गेय पद शैली काव्य - कृष्ण गीतावली, गीतावली ।
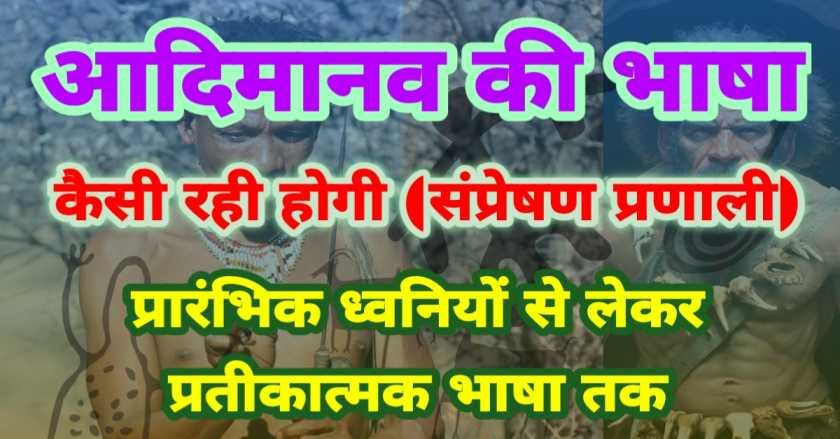





इस पोस्ट पर टिप्पणियाँ अक्षम हैं।